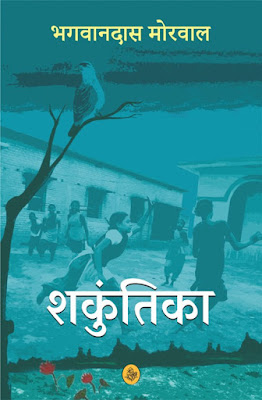स्वराज्य का सपना और प्रेमचंद ।
डॉ. मनीष कुमार मिश्रा
सहायक प्राध्यापक – हिन्दी
विभाग
के. एम. अग्रवाल
महाविद्यालय
कल्याण (पश्चिम), महाराष्ट्र
हिन्दी पट्टी के लोगों के लिए सचमुच यह गर्व का
विषय है कि उनके पास प्रेमचंद जैसा कद्दावर कथाकार “है” । एक ऐसा कथाकार जिसने
भारतीय साहित्य की अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बनाया । प्रेमचंद ने जो लिखा वो
लोगों को अपना सा लगा । हिन्दी पट्टी को साहित्य के मंच से समाज सुधार के लिए
वैचारिक स्तर पर आंदोलित करने वाले प्रेमचंद प्रमुख और अगुआ लेखक हैं ।
हिन्दी पाठकों की जमीन प्रेमचंद के पूर्व
जासूसी और अइयारी उपन्यासों से देवकीनंदन खत्री जैसे लेखक कर चुके थे । इन
उपन्यासों की लोकप्रियता का आलम यह था कि लोगों ने इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए
हिन्दी सीखी । कल्पना, जासूसी, ऐय्यारी, तिलिस्म की दुनिया
में भ्रमण करने वाले इन पाठकों को यथार्थ की ठोस जमीन पर समाज में व्याप्त
बुराइयों के खिलाफ़ वैचारिक स्तर पर गंभीर बनाना आसान नहीं था । यह वैसा ही था
जैसे दिनभर अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने-फ़िरने वाले किसी बालक का अचानक स्कूल में
दाखिला करा देना । दाख़िला कराना आसान है लेकिन बच्चे के अंदर अनुशासन और अध्ययन
रुचियों का निर्माण कराना कठिन है । इस कठिन कार्य को प्रेमचंद ने कर दिखाया ।
प्रेमचंद
इसलिए नहीं बड़े लेखक हैं कि उन्होने बड़ा लोकप्रिय साहित्य लिखा अपितु समाज के लिए
उपयोगी साहित्य को लिखना एवं उसे लोकप्रिय बनाने के लिए, प्रेमचंद
को अधिक याद किया जायेगा । प्रेमचंद ने
हिन्दी पट्टी के पाठकों की रुचियों का परिमार्जन किया । समाज और समाज की समस्याएँ
जो कि साहित्य के हाशिये पर थी उसे केंद्र में स्थापित करने का श्रेय प्रेमचंद को
है । 1918 से लेकर 1936 तक के समय में प्रेमचंद ने बेहतरीन कथा साहित्य लिखा ।
हंस जैसी पत्रिका का संपादन किया । उर्दू और हिन्दी के बीच में एक सेतु बनाने का
कार्य भी प्रेमचंद ने किया । अपने समय के दबाव के बावजूद अपनी रचना को नया कलेवर दिया
।
प्रेमचंद के प्रशंसकों में पंडित
जवाहरलाल नेहरू भी एक थे । अपूर्वानंद अपने आलेख में लिखते हैं कि, “नेहरू ने
आर. के. करंजिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हम सब गाँधी-युग की संतान हैं।
हिन्दी साहित्य में किसी प्रेमचंद-युग की चर्चा नहीं होती, उर्दू
साहित्य में भी शायद नहीं। लेकिन यह कहना बहुत ग़लत न होगा कि अज्ञेय हों या
जैनेंद्र या और भी लेखक, वे प्रेमचंद-युग की संतान हैं।’’1 प्रेमचंद
ने सिर्फ़ गाँव-जवार को ही अपने साहित्य में चित्रित नहीं किया अपितु उनके
साहित्यिक क़नात के नीचे गाँव और शहर दोनों थे । शायद यही कारण था कि अपने समय
के समाज को अधिक व्यापक रूप में वो चित्रित कर सके ।
प्रेमचंद
का समय आंतरिक जटिलताओं के संघर्ष का समय था । हिन्दी – उर्दू का झगड़ा चरम पर था ।
एक तरफ़ अल्ताफ हुसैन हाली तो दूसरी तरफ़ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी – अपनी
पताका संभाले हुए थे । बंगाल का विभाजन हो चुका था। महात्मा गांधी भारत की आज़ादी
के नये नायक के रूप में लोकप्रिय हो रहे थे । गहरे उपनिवेशवाद की छाप गाँव से लेकर
शहर तक दिखाई पड़ रही थी । यद्यपि प्रेमचंद के गावों में उसतरह की कुलबुलाहट नहीं
थी जैसी कि आज़ादी के तुरंत बाद फणीश्वरनाथ रेणु के “मैला आँचल” में दिखाई पड़ती है
। फ़िर भी बहुत कुछ था जो बदल रहा था । रेलवे,
फैक्ट्रियाँ, सड़कें, चीनी मिलें, सिनेमा,
अंग्रेज़ों के वफ़ादार जमीदार, रायसाहब इत्यादि के ताने-बाने के बीच समाज में बदलाव और
संघर्ष की एक आंतरिक धारा थी । इसकी एक
झलक किसानों के अंदर पनप रहे विद्रोह में भी देखी जा सकती है । रमा शंकर सिंह
लिखते हैं कि “बीसवीं शताब्दी के शुरुआती
दशकों में अवध में किसान आंदोलनों की श्रृंखला चल पड़ी थी। प्रतापगढ़ में बाबा
रामचंद्र किसानों से कह रहे थे कि वे अंग्रेजों को टैक्स न दें।“2
जगह-जगह छापे खाने खुल रहे थे ।
तरह-तरह की पत्र – पत्रिकाओं के माध्यम से समाज प्रबोधन का कार्य हो रहा था । राजा
रवि वर्मा जैसे कलाकार मंदिरों में कैद देवी-देवताओं को पोस्टर चित्रों के माध्यम
से घर-घर पहुंचा चुके थे । अछूतानंद जैसे नायक दलित समाज को आंदोलित कर रहे थे तो
डॉ. भीमराव आंबेडकर अपनी शिक्षा पूरी कर के भारत आ चुके थे । स्त्रियाँ शिक्षित हो
रहीं थी । उनके अधिकारों एवं शिक्षा को लेकर पक्षधरता बढ़ रही थी । 1894 के भूमि
अधिग्रहण क़ानून का विरोध और दमन दोनों हुआ । ‘जालियावाला
बाग’ जैसा जघन्य हत्याकांड अंग्रेज़ सरकार पहले ही कर चुकी थी
। इन तमाम घटनाओं के बीच से प्रेमचंद सेवा सदन, गोदान
और रंगभूमि जैसे उपन्यास लिखते हैं । प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिस तरह
से ब्रिटिश सरकार उपनिवेशवाद की जड़ों को भारत में जमा रही थी उसका एक व्यापक चित्र
प्रेमचंद के साहित्य में मिलता है ।
स्वामी
दयानंद सरस्वती का “आर्य समाज” जिस तरह से देश में सक्रिय था उससे प्रेमचंद भी
प्रभावित हुए । समाज में व्याप्त वेश्यावृत्ति की समस्या का निराकरण जिस तरह वे
“सेवा सदन” बनाकर दिखाते हैं, उससे उनपर आर्य समाज के प्रभाव को साफ़ देखा जा सकता है
। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्रभाव सिर्फ़ आर्य समाज का नहीं था । इस संदर्भ
में रमा शंकर सिंह अपने लेख में लिखते हैं कि,“विक्टोरियन
नैतिकताबोध से भारतीय समाज के ऊपर कानून लाद दिए गए थे और भारतीय पुरुष समाज
सुधारक जैसे मान चुके थे कि स्त्री का उद्धार करना उनका पुनीत कर्तव्य है।’’3 इन्हीं
सब के बीच प्रेमचंद ‘साहित्य के समाज’ और ‘समाज के
साहित्य’ दोनों को बदल रहे थे । उनके इस बदलाव को समाज ने भी स्वीकार किया क्योंकि वह
कोई वैचारिक या काल्पनिक बदलाव मात्र नहीं था । इस बदलाव का एक ‘अंडर
करेंट’ समाज महसूस कर रहा था जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है
।
प्रेमचंद लेखन की शुरुआत उर्दू से
करते हैं । उनकी कृतियों को अंग्रेज़ सरकार प्रतिबंधित करती है । प्रेमचंद सहज,सरल और
सपाट भाषा में लिखते हैं ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके
। वे प्रगतिशील विचारों के अगुआ बनते हैं । साहित्य को उस मशाल की संज्ञा
देते हैं जो राजनीति के आगे-आगे चलकर उसका पथ प्रदर्शन करे । 1906 से 1936 तक
लिखा गया उनका पूरा साहित्य अपने समय और समाज की त्रासदी का बयान है । मंगलसूत्र
उपन्यास वो पूरा नहीं कर सके । कफ़न उनकी लिखी अंतिम कहानी साबित हुई ।
अंतिम पूर्ण उपन्यास के रूप में उन्होने गोदान जैसी सशक्त रचना दी । कमल किशोर
गोयनका ने उनकी 25 से 30 लघु कहानियाँ भी खोजी हैं जो पाठकों के लिए सहज रूप से
उपलब्ध हो चुकी है । बलराम अग्रवाल अपने आलेख – प्रेमचंद की लघु कथा रचनाएँ में
इसकी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं ।4 प्रेमचंद ने तीन सौ के आस-पास
कहानियाँ लिखीं । अधिकांश कहानियों के केंद्र में समाज की कोई न कोई समस्या है । पंच
परमेश्वर, पूस की रात, ठाकुर का कुआं , नमक का
दरोगा, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, आभूषण, कामना, बड़े भाई
साहब, सत्याग्रह, घासवाली और कफ़न जैसी उनकी कहानियाँ अधिक लोकप्रिय रही
हैं । लेकिन उनकी समस्त कहानियों में समस्याओं और सूचनाओं का इतना अंबार है कि
हिन्दी पट्टी के समाज और समाज मनोविज्ञान को समझने में ये बहुत सहायक हैं । साहित्य
को सामाजिक सरोकारों एवं प्रगतिशील मूल्यों के साथ जोड़कर प्रेमचंद ने एक नई
परिपाटी शुरू की ।
डॉ. कमल किशोर गोयनका ने तमाम प्रमाणों
एवं साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया है कि प्रेमचंद को जिस तरह रामविलास शर्मा
जी गरीब और जीवन भर तंगी में ही रहने की बात करते हैं वह गलत है ।5 प्रेमचंद
की माली हालत हमेशा ठीक ठाक रही । लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हमेशा
ही उस शोसित-वंचित की चिंता की जो ब्रिटिश कालीन उपनिवेशिक समाज में सम्पन्न वर्ग
द्वारा निचोड़ा जा रहा था । प्रेमचंद का समय कई विचारधाराओं के उत्थान का भी समय था
। निश्चित था कि प्रेमचंद भी किसी न किसी रूप में इनसे प्रभावित होते । किसान
आंदोलन, भूमि अधिग्रहण कानून, रुसी
क्रांति, लियो टोल्सटाय,
गांधी और डॉ आंबेडकर की विचारधाराओ ने प्रेमचंद को प्रभावित
किया । 1927 से डॉ. अम्बेडकर के आंदोलनों की तीव्रता ने पूरे देश को प्रभावित किया
। प्रेमचंद की कई महत्वपूर्ण कहानियाँ इसी के बाद ही आयीं । जैसे कि “ठाकुर का
कुँआ”, “दूध का दाम”,
“सद्गति” और उनकी अंतिम कहानी “कफ़न” ।
यद्यपि कफ़न को लेकर दलित साहित्य समीक्षकों ने प्रेमचंद की कड़ी निंदा भी की है
लेकिन वह एक ख़ास नजरिये से देखना भर है, उसमें
समग्रता का अभाव है ।
31 जुलाई 1880 को जन्में प्रेमचंद ने 08 अक्टूबर 1936 को
अंतिम सांस ली । तमाम सामाजिक,राजनीतिक परिस्थितियों और विचारधाराओं के बीच प्रेमचंद
जिस भारत की संकल्पना को अपने साहित्य के माध्यम से साकार कर रहे थे वहाँ समतामूलक
सर्वसमावेशी स्वराज्य का सपना था । उनकी राष्ट्रियता की छवि में जन्मगत वर्ण
व्यवस्था की गंध तक स्वीकार्य नहीं थी । नवजागरण की पृष्ठभूमि से उठे सारे
सवालों को वे अपने साहित्य के माध्यम से उठा रहे थे । राष्ट्रीय रंगमंच पर गांधी
और आंबेडकर के विचारों से उस भारत को गढ़ना चाह रहे थे जिसमें मनुष्यता महत्वपूर्ण
है । चित्त की उदारता सिर्फ़ विचारों और ग्रंथों तक सीमित न होकर वह व्यवहार का
हिस्सा बने, यह प्रेमचंद की इच्छा थी । उपनिवेशिक दबाव और प्रभाव के
बीच भारत का जो छविकरण “Land of Religion
and Philosophy” के रूप में किया जा रहा
था वह इस भारत की समग्र आत्मा का प्रतिनिधित्व नहीं था । उसमें वर्तमान के
परिप्रेक्ष्य में भविष्य की संकल्पना स्पष्ट नहीं थी ।
प्रेमचंद ने साहित्य को अपने समाज और
समय की धड़कन में बदलते हुए नायकत्व की पूरी परिपाटी को बदल दिया । मनुष्यता को
साहित्य के केंद्र में स्थापित किया । अनुभूति की जीवंतता को प्रेमचंद ने
महत्वपूर्ण माना । उत्तर भारत की स्मृतियों,
अनुभूतियों, रंग, रूप, रस और गंध सबकुछ प्रेमचंद ने अपने साहित्य में समेटा ।
भूत और भविष्य की चिंता को व्यर्थ का भार मानने वाले प्रेमचंद अपने वर्तमान को
पूरी समग्रता से चित्रित करते हैं । समाज के दबे – कुचले और शोषित वर्ग को
मनुष्यता का स्वर प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से ही दिया । कठिनाइयों से
लड़ने के लिये गति और बेचैनी को प्रेमचंद महत्वपूर्ण मानते थे । वे एक ऐसे साहित्य
के हिमायती थे जो संघर्ष के लिये बेचैनी पैदा करे । प्रेमचंद के साहित्य में समय
विशेष का लोक चित्त और उसका इतिहास धड़कता है ।
प्रेमचंद ने गाँव के जिस जीवंत परिवेश का चित्रण करते हैं
उसने उनकी बाद की पीढ़ी के लिए एक रास्ता प्रसस्त किया । सरोकारजन्य साहित्य की परिपाटी
उन्हीं की देन है । प्रेमचंद के बाद शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वरनाथ
रेणु, चन्द्र्किशोर जायसवाल, अमरकांत, संजीव, रामधारी सिंह
दिवाकर, राकेश कुमार सिंह, मैत्रयी पुष्पा, काशीनाथ सिंह, देवेन्द्र, अखिलेश, महेश कटारे, सत्यनारायण
पटेल और शिवमूर्ति जैसे कथाकारों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया । प्रेमचंद की परंपरा में कई शाखाएँ मानी जा सकती हैं जो उनके
विचारों को अग्रगामी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।
प्रोफ़ेसर चित्त रंजन मिश्र के अनुसार
गोरखपुर के बाले मियाँ के मैदान में गाँधी
जी का भाषण सुनने के बाद ही उन्होने सरकारी नौकरी से 1921 में त्यागपत्र दिया । बाद
में वे लमही अपने गाँव लौट गये थे । प्रेमचंद के साहित्य की एक महत्वपूर्ण बात यह भी
है कि प्रेमचंद अपने पात्रों की आर्थिक स्थिति का वर्णन अवश्य करते हैं । न केवल वर्णन
करते हैं अपितु उस पैसे के आने और जाने के संदर्भ को भी बड़े सलीके से चित्रित करते
हैं । यह अर्थ उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव लाता है, उसकी सोच
को किस तरह प्रभावित करता है, इसका व्यापक चित्र खींचते हैं । कबीर और तुलसी के बाद संभवतः
प्रेमचंद का ही पाठक वर्ग सबसे बड़ा हो । इन पाठकों तक प्रेमचंद धर्म और कर्मकांडों
के माध्यम से नहीं अपितु धार्मिक पाखंडों की पोल खोलते हुए पहुँचते हैं । सामाजिक विसंगतियों
की गाँठों को लेकर अपने पाठकों तक जाते हैं । प्रेमचंद ख़ुद भी अपने आप को वैचारिक स्तर पर माँजते
रहे । सन 1916 से 1936 तक आते-आते प्रेमचंद में यह बदलाव साफ़ दिखायी पड़ता है । प्रेमचंद
की हिन्दी वह हिंदुस्तानी थी जिसकी बात गाँधी जी करते थे । ठेठ जन की भाषा को उन्होने
अपनाया ।
फ़िल्मों की दुनियाँ में भी प्रेमचंद
ने क़दम तो रक्खा लेकिन वे यहाँ से निराश अधिक हुए । प्रेमचंद की लिखी फिल्म ‘द मिल मजदूर’ मुंबई में
5 जून 1939
को इंपीरियल सिनेमाघर में
लंबी लड़ाई के बाद रिलीज हुई थी। वैसे तो
यह फिल्म 1934 में ही बनकर
तैयार हो चुकी थी, लेकिन उस समय मुंबई के बीबीएफसी (बॉम्बे बोर्ड ऑफ
फिल्म सर्टिफिकेशन) ने इसे प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं प्रदान की । उन्हें
यह लगता था कि फ़िल्म मजदूरों को बरगला सकती है और वे हड़ताल कर सकते हैं । तत्कालीन
सेंसर बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल बेरामजी जीजीभाई मुंबई मिल
एसोसिएशन के भी अध्यक्ष थे, वे इस फ़िल्म को मिल
एसोसिएशन के हितों के अनुकूल नहीं समझते थे । 1937 में
बीबीएफसी का फिर से गठन हुआ और नए सदस्य चुने गए। तब जाकर इस फ़िल्म को प्रदर्शित
करने का रास्ता साफ हुआ । यह फ़िल्म प्रेमचंद की मृत्यु के बाद प्रदर्शित हुई ।
प्रेमचंद खेतिहर भारतीय जनमानस के सबसे बड़े और सबसे अधिक
स्वीकृत कथाकारों में रहे हैं । उनके साहित्य के माध्यम से बहस और चिंतन की गुंजाइस
लगातार बनी हुई है । वे अपनी किरदार निगारी में अद्भुद रहे । प्रेमचंद का साहित्य
अपने समय की वास्तविकता की तलाश है । इस तलाश की केन्द्रिय इकाई मानवीयता है ।
प्रेमचंद ने अपने पाठकों के साथ जिस विश्वास की परंपरा का निर्माण किया, उतनी मज़बूत
और व्यापक कड़ी उनके बाद का कोई भी लेखक अभी तक नहीं बना पाया है । अपने समय के संघर्ष
का मानो प्रेमचंद इक़बालिया बयान दर्ज़ कर रहे हों ।
संदर्भ :
1. प्रेमचंद 140 : सातवीं कड़ी : हिन्दी साहित्य में
प्रेमचंद-युग की चर्चा क्यों नहीं? –अपूर्वानंद https://www.satyahindi.com/literature/140-years-of-premchand-part-7
2. प्रेमचंद का सूरदास आज भी ज़मीन हड़पे जाने का विरोध कर
रहा है और गोली खा रहा है! – रमा शंकर सिंह, https://junputh.com/open-space/rama-shankar-singh-on-premchand-jayanti
3. वही
4. प्रेमचंद की लघु कथा रचनाएँ – बलराम अग्रवाल https://www.bharatdarshan.co.nz/magazine/articles/606/premchand-ki-laghukatha-rachanayein
5. प्रेमचंद गरीब थे, यह
सर्वथा तथ्यों के विपरीत है – रोहित कुमार ‘हैप्पी’, https://www.bharatdarshan.co.nz/magazine/articles/600/grib-nahi-the-premchand.html?